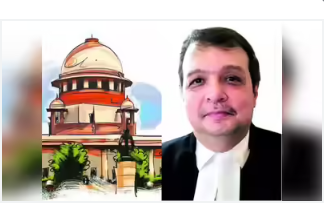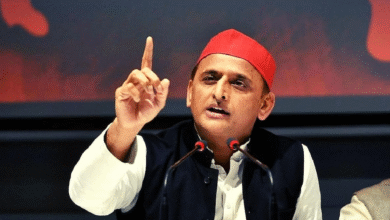कोरोना के दौर में दुनिया भर में मीडिया पर कसता सरकारों का शिकंजा

कोरोना वायरस ने न केवल विश्व के सभी देशों को अप्रत्याशित झटका दिया है बल्कि हर सरकार को बुरी तरह से झकझोर कर भी रख दिया है.
लगभग सभी देशों ने पिछले साल भर के दौरान कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने की कोशिशें तो की हैं. ये कुछ हद तक सफल भी हुईं, मगर उसके साथ-साथ ऐसे भी कदम उठाए हैं, जिन्हें प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ख़तरा माना जा रहा है.
शुरू से ही यह साफ था कि कोई भी देश इस तरह की आपदा के लिए तैयार नहीं था. पर जब कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा और सरकारें चुनौती से निबटने में नाकाम रहीं तो ब्राजील से लेकर पाकिस्तान तक में उनकी आलोचना होने लगी.
एक तरफ समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविज़न चैनलों और वेबसाइटों पर आ रहे समाचार स्थिति की भयावहता और वास्तविकता का दिन-रात वर्णन कर रहे थे. दूसरी तरफ, सार्वजनिक स्तर पर निंदा बढ़ती जा रही थी. इससे न केवल अलोकतांत्रिक शासकों को बल्कि कई लोकतांत्रिक देशों में सत्तारूढ़ नेताओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई.
सच बताने की जगह इसे छिपाने का दबाव डाला गया
ऐसी परिस्थिति में मीडिया संगठनों को विश्वास में लेकर जनता को सही जानकारी देने की जगह, इन सरकारों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की. नतीजतन, समाचार संस्थाओं के खि़लाफ कानूनी कदम उठाए गए और पत्रकारों पर हमले होने लगे.
सार्वजनिक चर्चा को नियंत्रित करने के लिए कई देशों में, स्वतंत्र मीडिया के पत्रकारों को प्रेस ब्रीफिंग तक पहुंच से वंचित कर दिया गया. आधिकारिक सूचना तक पहुंच को सीमित कर दिया गया और मीडिया संगठनों को सरकारी आँकड़ों को ही प्रकाशित करने के लिए बाध्य किया गया.
दुनिया में ऐसे उत्पीड़न के 600 मामले
पिछले वर्ष फरवरी से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए 1950 में स्थापित संपादकों, मीडिया प्रबंधकों और प्रमुख पत्रकारों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्यूट (आईपीआई) ने प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन और पत्रकारों पर हो रहे हमलों के आंकड़े जमा करना शुरू किया.
आईपीआई के कोविड-19 प्रेस फ्रीडम ट्रैकर के अनुसार अब तक विश्व भर में 600 से अधिक ऐसे मामले उजागर हुए हैं. इनमें या तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है या फिर पत्रकारों पर शारीरिक हमले या जरूरत से ज्यादा सख़्त कार्रवाइयाँ हुई हैं.
हालांकि प्रेस स्वतंत्रता ट्रैकर में सभी उल्लंघनो के आँकड़े संकलित करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है. एकत्रित आँकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता को सरकारों के कदमों से बहुत धक्का लगा है. नतीजतन आम लोग प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी से वंचित रह गए हैं.
आंकड़े दर्शाते हैं कि 34 प्रतिशत मामलों में पत्रकारों पर हमले हुए, जबकि 33.5 प्रतिशत घटनाएं पत्रकारों की गिरफ्तारी से संबंधित हैं या जिनमें सरकारों ने पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उल्लंघन के सभी मामलों में से लगभग 14 प्रतिशत सूचना के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित हैं.
आँकड़ों के क्षेत्रीय विभाजन से पता चलता है कि गिरफ्तारी और आरोपों से संबंधित उल्लंघन के सबसे अधिक मामले एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हुए. वहीं पत्रकारों पर शारीरिक हमले और धमकियाँ यूरोप में सबसे अधिक दर्ज हुईं.
एशिया-प्रशांत में एक तिहाई मामले
कुल मिलाकर, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महामारी से जुड़े लगभग 200 उल्लंघन सामने आए. इनमें से 107 चार दक्षिण एशियाई देशों – बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और नेपाल से थे. इन देशों में 71 पत्रकार या तो गिरफ्तार किए गए या उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई. वहीं 32 मामलों में पत्रकारों पर शारीरिक और मौखिक हमले हुए.
दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा उल्लंघन और हमले भारत में हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार, भारत में 84 मामले सामने आए. विभिन्न कानूनों के तहत भारत में 56 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, या उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. इसके अलावा 23 पत्रकार हमलों के शिकार हुए.
बांग्लादेश और नेपाल में कई पत्रकार गिरफ्तार हुए, और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए.
बांग्लादेश सरकार ने महामारी के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप कुछ पत्रकारों और एक कार्टूनिस्ट सहित 11 लोगों पर लगाया, मगर इनमें से केवल दो को ही गिरफ्तार किया जा सका क्योंकि बाकी पत्रकार विदेश में हैं.
नेपाल में सरकार ने मीडिया को आवश्यक सेवा घोषित किए जाने के बाद भी पुलिस ने छह पत्रकारों को हिरासत में लिया और चार पत्रकारों पर हमले हुए.
पाकिस्तान में उल्लंघन का जो सबसे भयावह मामला सामने आया उसमें अर्धसैनिक बलों ने दो पत्रकारों को बुरी तरह प्रताड़ित किया था. इन पत्रकारों ने अफगानिस्तान की सीमा के करीब एक क्वारंटीन सेंटर में बुरे हालात पर रिपोर्टिंग की थी.
सईद अली अचकजई और अब्दुल मतीन अचकजई ने आरोप लगाया कि उन्हें फ्रंटियर कोर के कमांड सेंटर में बुलाया गया और आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स को सौंप दिया गया. उन्हें जेल ले जाया गया और प्रताड़ित किया गया.

इमेज स्रोत,GETTY IMAGES
भारत के मामले
महामारी के बारे में रिपोर्ट करने से रोकने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के तरीके अपनाए. सरकार ने इस बात का पुरज़ोर प्रयास किया कि समाचार संस्थाएं केवल सरकारी आंकड़ों को ही प्रकाशित करें.
पिछले वर्ष 31 मार्च को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह समाचार संस्थाओं को निर्देश दे कि वे कोविड के बारे में उन आँकड़ों को प्रकाशित न करें जिन्हें सरकार ने जारी नहीं किया हो, मगर न्यायालय ने सरकार के इस अनुरोध को ठुकरा दिया.
अधिकांश पत्रकारों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ केस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की नाकामी और स्थानीय अधिकारियों की कमियों को छिपाने की कोशिशों को उजागर किया था.
मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश में छह पत्रकारों के खिलाफ 10 मामले इसलिए दर्ज किए गए क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार की अचानक तालाबंदी के कारण फंसे हुए प्रवासी कामगारों के बीच फैल रही भुखमरी, और स्थानीय प्रशासन की खामियों के बारे में समाचार प्रकाशित किए.
एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पत्रकारों के खिलाफ केस तब दर्ज किए गए जब स्थानीय नेताओं और इन पत्रकारों के बीच रिपोर्टिंग तो लेकर विवाद हो गया.
इन सब के बीच एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और प्रदेश की सरकारों से प्रेस को परेशान करने के लिए कानूनी साधनों का उपयोग बंद करने का आग्रह किया.
कोविड से जुड़े समाचार पर नियंत्रण करने की कोशिश के अलावा भारत में केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जो और कदम उठाए हैं उनको लेकर भी पत्रकार बिरादरी में चिंता है.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अनुसार जनवरी 2021 में पत्रकारों पर 15 से अधिक हमले हुए और यह सभी हमले तब हुए जब पत्रकार कोरोना संक्रमण के दौर में ही चल रहे किसान आंदोलन कवर करने गए थे.

इमेज स्रोत,PIB
भारत में नए नियम
दो माह पहले, भारत सरकार ने आइटी एक्ट 2000 के तहत इनफार्मेशन टेकनोलॉजी (गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटीएस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 जारी किये हैं.
पत्रकारिता से जुड़े लोगों का मानना है कि ये नियम देश में प्रेस की स्वतंत्रता को न केवल कमजोर करेंगे साथ ही, समाचार संगठनों पर भारी वित्तीय और कानूनी बोझ डालेंगे, जिसे छोटे और मध्यम स्तर के समाचार संगठन नहीं उठा सकेंगे.
नए नियमों के अनुसार हर मीडिया संगठन को एक अनुपालन अधिकारी (कम्पलायंस ऑफ़िसर) की नियुक्ति करनी होगी जो पाठकों की हर शिकायत का 15 दिन में जवाब देगा.
निर्देशों के अनुसार, मीडिया संगठन मिलकर एक स्व-नियामक समिति या सेल्फ़ रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना करेंगे जो पाठकों की शिकायत पर कार्रवाई करेगी. और इन सब के ऊपर भारत सरकार के सचिवों की एक समिति होगी जो कि उस तक पहुंची शिकायतों पर कदम उठाएगी.
समाचार संगठन सरकार के इस नियम से बहुत ही आशंकित हैं और कुछ ने इन नियमों के विरुद्ध दिल्ली और केरल उच्च न्यायालयों में याचिकाएं भी दायर की हैं.
(रवि प्रसाद, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट में एडवोकेसी के निदेशक हैं)