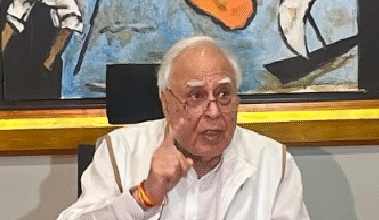राजद्रोह: क्या ब्रिटिश राज का दमनकारी क़ानून वर्तमान भारत में प्रासंगिक है?


इमेज स्रोत,RAMESH LALWANI/GETTYIMAGES
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो टीवी चैनलों के ख़िलाफ़ राजद्रोह के आरोप में आंध्र प्रदेश पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकते हुए कहा कि राजद्रोह से सम्बंधित आईपीसी की धारा 124ए की व्याख्या करने के ज़रुरत है.
अदालत ने ये भी कहा कि इस धारा के इस्तेमाल से प्रेस की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले असर के मद्देनज़र भी इस व्याख्या की ज़रुरत है.
आंध्र प्रदेश पुलिस ने दो तेलुगू न्यूज़ चैनलों- टीवी 5 और एबीएन चैनल के ख़िलाफ़ 14 मई को राजद्रोह का मुक़दमा दायर किया था. इन चैनलों पर आरोप है कि उन पर प्रसारित कार्यक्रमों के दौरान लोक सभा सांसद रघुराम कृष्णम राजू ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी की आलोचना की.
एफ़आईआर में राजू को पहले, टीवी5 और एबीएन को क्रमश: दूसरे और तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है. राजू सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के ही एक विद्रोही नेता हैं और इस मामले में उनकी गिरफ़्तारी होने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.
इन चैनलों की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में कहा कि आंध्र पुलिस की यह एफ़आईआर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुंह बंद करने का प्रयास है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है.
चैनलों के वकीलों ने यह भी कहा कि 30 अप्रैल को दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि कोविड संकट के सन्दर्भ में शासकीय मसलों पर की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई पर अंकुश लगाने की ज़रुरत है.
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके विचार में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के प्रावधानों के दायरे और मापदंडों की व्याख्या की आवश्यकता होगी. ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के समाचार और सूचना पहुँचाने के सन्दर्भ में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस व्याख्या का हिस्सा वे समाचार या सूचनायें भी होंगी जिनमे देश के किसी भी हिस्से में प्रचलित शासन की आलोचना की गई हो.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक आंध्र प्रदेश पुलिस इन चैनलों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती.
विनोद दुआ के ख़िलाफ़ केस ख़ारिज
3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश के शिमला में दर्ज देशद्रोह के मामले को ख़ारिज कर दिया. दुआ के ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय भाजपा नेता ने उनके यूट्यूब शो को लेकर मामला दर्ज कराया था.
दुआ पर देशद्रोह सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था और भाजपा नेता ने दावा किया था कि दुआ ने 30 मार्च, 2020 को अपने 15 मिनट के यूट्यूब शो में अजीबोगरीब आरोप लगाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिए “मौतों और आतंकी हमलों” का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.
इस मामले ने अदालत ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार केदार नाथ सिंह के फ़ैसले के तहत सुरक्षा का हकदार है जिसमे धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराध के दायरे को परिभाषित किया गया है.
क्या है राजद्रोह का क़ानून?
भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी और तरह से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या भारत में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का आरोपी है.
राजद्रोह एक ग़ैर-जमानती अपराध है और इसमें सज़ा तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है.
केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124ए के बारे में कहा था कि इस प्रावधान का इस्तेमाल “अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति, या क़ानून और व्यवस्था की गड़बड़ी, या हिंसा के लिए उकसाने वाले कार्यों” तक सीमित होना चाहिए.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने अपने फ़ैसले में आईपीसी के तहत राजद्रोह क़ानून की वैधता को बरकरार रखा था और इसके दायरे को भी परिभाषित किया था. अदालत ने कहा था कि धारा 124ए केवल उन शब्दों को दंडित करता है जो क़ानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की मंशा या प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं या जो हिंसा को भड़काते हैं. उसी समय से इस परिभाषा को धारा 124ए से संबंधित मामलों के लिए मिसाल के तौर पर लिया जाता रहा है.

इमेज स्रोत,NENOV/GETTY IMAGES
मीडिया और राजद्रोह
पिछले कुछ महीनों में समय समय पर मीडिया और पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह के मुक़दमे दर्ज किये गए हैं.
इसी साल जनवरी में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर सहित छह पत्रकारों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. यह मामला एक शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया था कि इन लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट्स और डिजिटल प्रसारण राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के लिए ज़िम्मेदार थे.
अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य लोगों पर राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया. कप्पन एक कथित सामूहिक बलात्कार मामले की रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे.
उसी महीने मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया. वांगखेम को 2018 में भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरएसएस, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने के लिए गिरफ़्तार किया गया था. मणिपुर उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2019 में उनके ख़िलाफ़ आरोपों को ख़ारिज करते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया था.

इमेज स्रोत,XAVIER GALIANA/GETTYMAGES
गिरफ़्तारी, चार्जशीट और दोष साबित करना
नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में साल 2015 में 30, 2016 में 35, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए.
2019 में देश में जो 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और 96 लोगों को गिरफ़्तार किया गया. इन 96 लोगों में से 76 आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई और 29 को बरी कर दिया गया. इन सभी आरोपियों में से केवल दो को अदालत ने दोषी ठहराया.
2018 में जिन 56 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया उनमे से 46 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर हुई और उनमें से भी केवल 2 लोगों को ही अदालत ने दोषी माना.
इसी तरह 2017 में जिन 228 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया उनमें से 160 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर हुई और उनमे से भी मात्र 4 लोगों को ही अदालत ने दोषी माना.
2016 में 48 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया और उनमें से 26 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर हुई और केवल 1 आरोपी को ही अदालत ने दोषी माना.
वहीं 2015 में इस क़ानून के तहत 73 गिरफ़्तारियां हुईं और 13 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर हुई लेकिन इनमें से एक को भी अदालत में दोषी नहीं साबित किया जा सका.
इसी तरह 2014 में 58 लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया लेकिन सिर्फ़ 16 के ख़िलाफ़ ही चार्जशीट दायर हुई और उनमें से भी केवल 1 को ही अदालत ने दोषी माना.
क्या राजद्रोह के क़ानून को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए?
पिछले कुछ सालों से इस बात पर बहस चल रही है कि क्या देशद्रोह कानून को खत्म कर देना चाहिए?
जुलाई 2019 में राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि “देशद्रोह के अपराध से निपटने वाले आईपीसी के तहत प्रावधान को ख़त्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है”.
साथ ही सरकार ने कहा कि “राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रावधान को बनाए रखने की आवश्यकता है”.
रेबेका जॉन सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आईपीसी की 124ए नाम की कोई धारा ही नहीं होनी चाहिए.
वह कहती हैं, “मेरा मानना है कि दिशानिर्देश तय करने से काम नहीं चलने वाला है. धारा के दिशा-निर्देश और मानदंड 60 के दशक में निर्धारित किए गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने केदार नाथ सिंह मामले का फ़ैसला सुनाया था. पांच दशक बाद भी हम उस फ़ैसले की मंशा और दायरे की ग़लत व्याख्या कर रहे हैं और हम अभी भी दिशानिर्देशों की तलाश में हैं. इसलिए मुझे लगता है कि इस क़ानून का क़ानून की किताब में होना ही इसके दुरुपयोग को जन्म देता है.”
जॉन मानती हैं कि इस क़ानून कि कितनी भी व्याख्या या पुनर्व्याख्या कर ली जाये “कोई तो होगा जो एफ़आईआर दर्ज करवाएगा और कोई अदालत होगी जो इसका संज्ञान लेगी”. उनका कहना है कि इस तरह का प्रावधान जिसे दुनिया के अन्य हिस्सों में क़ानून की किताब से हटा दिया गया है उसे भारत में भी क़ानून की किताब में नहीं रहना चाहिए.
राजद्रोह के बारे में की गई हालिया टिप्पणियों का स्वागत करते हुए जॉन कहती हैं कि “आख़िरकार संसद को यह सुनिश्चित करना होता है कि धारा को क़ानून की किताब से हटा दिया जाए.”
कॉलिन गोंसाल्विस सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील है और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के संस्थापक भी हैं.
गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह से सम्बंधित उस लंबित याचिका में याचिकर्ताओं के प्रतिनिधि भी हैं जिसमे कहा गया है कि राजद्रोह का क़ानून नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट के एक तीन जजों के बेंच ने राजद्रोह के दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सहमति जताई है.
बीबीसी से बात करते हुए गोंसाल्विस ने कहा कि राजद्रोह का क़ानून लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है.
वे कहते हैं कि “1960 के दशक में केदार नाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उस याचिका पर था जिसमें राजद्रोह की धारा को रद्द करने की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने क़ानून की परिभाषा को संकुचित बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए जो इस प्रावधान में नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ शब्द ही नहीं अस्थिर करने के लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी राजद्रोह लागू होगा. लेकिन एक संवैधानिक मामले में, विशेष रूप से आपराधिक न्याय के मामले में, यह गलत दृष्टिकोण है.”
गोंसाल्विस के अनुसार, करतार सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब क़ानून की कोई धारा अस्पष्ट है तो उस धारा को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए.
क़ानून की अस्पष्टता और ज़मीनी हक़ीक़त
गोंसाल्विस कहते हैं कि “आपराधिक कानून की किसी भी धारा को अस्पष्ट होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे इस बात की व्याख्या का दायरा बढ़ जाता है कि अपराध क्या है.”
उदाहरण के तौर पर गोंसाल्विस कहते हैं कि “मान लीजिए कि किसी पुलिस स्टेशन का एक एसएचओ इंकलाब जिंदाबाद का पोस्टर देखता है, मान लीजिए कि वह एक पत्रकार को देखता है जो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है, मान लीजिए कि वह एक कार्टूनिस्ट को देखता है, जिसने किसी राजनीतिक व्यक्ति का कार्टून बनाया है. तो वह केवल क़ानून की धारा के हिसाब से चलेगा. अगर वह आईपीसी के अनुसार कार्रवाई करता है तो वह केदार नाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं पढ़ेगा.”
उनके अनुसार राजद्रोह की धारा 124ए में अदालत ने जो शब्द जोड़े वे यह थे- “बशर्ते कि शब्दों के साथ राज्य के ख़िलाफ़ हिंसक कार्रवाई हो”.
वह कहते हैं, “एसएचओ इस फैसले को पढ़ने की परेशानी क्यों उठाएंगे? वह उस आईपीसी के हिसाब से चल रहे हैं जिसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया है.”
गोंसाल्विस का मानना है कि अगर आपराधिक क़ानून की कोई धारा अस्पष्ट है तो लोगों को उस धारा के अधीन नहीं किया जा सकता जो उन्हें आजीवन जेल में डाल सकती है.
वह कहते हैं कि जितने भी पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है उनमें से एक भी पत्रकार ने हिंसक कृत्य नहीं किया फिर भी उन्हें गिरफ़्तार किया गया.
राजद्रोह के क़ानून में “भारत में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उत्तेजना या असंतोष को उत्तेजित करने” के प्रयास की बात की गई है.
गोंसाल्विस पूछते हैं, “असंतोष का क्या अर्थ है? क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे सरकार से नफ़रत है? क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे प्रधानमंत्री से नफ़रत है? क्या मैं यह नहीं कह सकता कि अमुक राजनेता भारत के इतिहास में सबसे बुरे हैं? यह सब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है.”
नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़े साफ़ दिखाते हैं कि राजद्रोह के अधिकतर मामलों में दोषी माना जाना तो दूर चार्जशीट तक नहीं दायर हो पाती. इस बात से क्या समझा जाये.
जॉन कहती हैं, ” ये मामले बड़े जोश के साथ दर्ज किए जाते हैं लेकिन जांच एजेंसियों के पास अक्सर कोई सबूत नहीं होते. यह क़ानून मूल रूप से लोगों में भय पैदा करता है और असंतोष को दबाने में सफल होता है.”
गोंसाल्विस कहते हैं, “यदि आप राजद्रोह क़ानून या यूएपीए को देखें तो सज़ा की दर कम है क्योंकि पुलिस को आरोपी को दोषी ठहराने में कोई दिलचस्पी नहीं है. पुलिस चाहती है कि एक व्यक्ति को बिना मुक़दमा शुरू हुए ही 5 साल जेल में रह ले. पुलिस केवल ज़मानत ख़ारिज कराना चाहती है. ज़मानत का विरोध होने पर आरोपी 3-4 साल तक सलाखों के पीछे रह सकता है. पत्रकार किशोर चंद्र एक साल तक जेल में रहे.”
रेबेका जॉन कहती हैं, “मुझे इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि मैं एक संविधान द्वारा शासित एक गर्वित, स्वतंत्र गणराज्य का हिस्सा हूं और फिर भी मुझे बताया गया है कि उस समय की सरकार के ख़िलाफ़ किसी तरह की आलोचना राजद्रोही हो सकती है. मुझे यह बहुत समस्यापूर्ण लगता है क्योंकि इस देश के नागरिक के रूप में मुझे किसी भी समय की किसी भी सरकार की आलोचना करने का अधिकार है. और यह राजद्रोही नहीं है.
जॉन कहती हैं कि यह कानून एक “औपनिवेशिक विरासत है” जिसे लागू करके औपनिवेशिक शक्तियों ने अपनी प्रजा को दबाने की कोशिश की.
“महात्मा गांधी इस का़ानून की सजा पाने वालों में से एक थे और निश्चित रूप से उस तरह के इतिहास और विरासत के साथ भारतीयों के रूप में हमें अपमानित महसूस करना चाहिए कि हमारी क़ानून की किताब में 124ए जैसा कानून मौजूद है.”
विधि आयोग का परामर्श पत्र
भारतीय विधि आयोग या लॉ कमीशन ने 2018 में राजद्रोह के ऊपर एक परामर्श पत्र जारी किया.
राजद्रोह के कानून को लेकर आगे क्या रास्ता निर्धारित किया जाना चाहिए इस पर लॉ कमीशन ने कहा कि “लोकतंत्र में एक ही गीत की किताब से गाना देशभक्ति का पैमाना नहीं है” और “लोगों को अपने तरीके से अपने देश के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए” और ऐसा करने के लिए “सरकार की नीति में ख़ामियों की ओर इशारा करते हुए कोई रचनात्मक आलोचना या बहस” की जा सकती है.
लॉ कमीशन ने कहा कि “इस तरह के विचारों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति कुछ के लिए कठोर और अप्रिय हो सकती है” लेकिन ऐसी बातों को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है. लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि “धारा 124ए केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे की मंशा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा और अवैध साधनों से सरकार को उखाड़ फेंकने की है”.
इस परामर्श पत्र में लॉ कमीशन ने कहा कि “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हर ग़ैर-ज़िम्मेदाराना प्रयोग को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है”.
साथ ही यह भी कहा कि तत्कालीन सरकार की नीतियों से मेल न खाने वाले विचार व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति पर राजद्रोह की धारा के तहत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए.
लॉ कमिशन ने कहा कि देश या उसके किसी विशेष पहलू पर अपशब्द कह देना देशद्रोह नहीं माना जा सकता है और साथ ही यह भी जोड़ा अगर देश सकारात्मक आलोचना के लिए खुला नहीं है तो ये आज़ादी से पहले और बाद के युगों के बीच का अंतर दर्शाता है. अपने स्वयं के इतिहास की आलोचना करने का अधिकार और ‘अपमान’ करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित अधिकार हैं.
परामर्श पत्र में कहा गया कि जबकि यह प्रावधान राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है इसका दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही यह भी कहा कि असहमति और आलोचना जीवंत लोकतंत्र में नीतिगत मुद्दों पर एक मजबूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं और इसीलिए अनुचित प्रतिबंधों से बचने के लिए स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति पर हर प्रतिबंध की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए.
लॉ कमीशन ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम ने दस साल पहले देशद्रोह क़ानूनों को समाप्त कर दिया था और ऐसा करते वक़्त कहा था कि वो देश ऐसे कठोर क़ानूनों का उपयोग करने का उदाहरण नहीं बनना चाहता. परामर्श पत्र में पूछा गया कि उस धारा 124ए को बनाये रखना कितना उचित है जिसे अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया था.